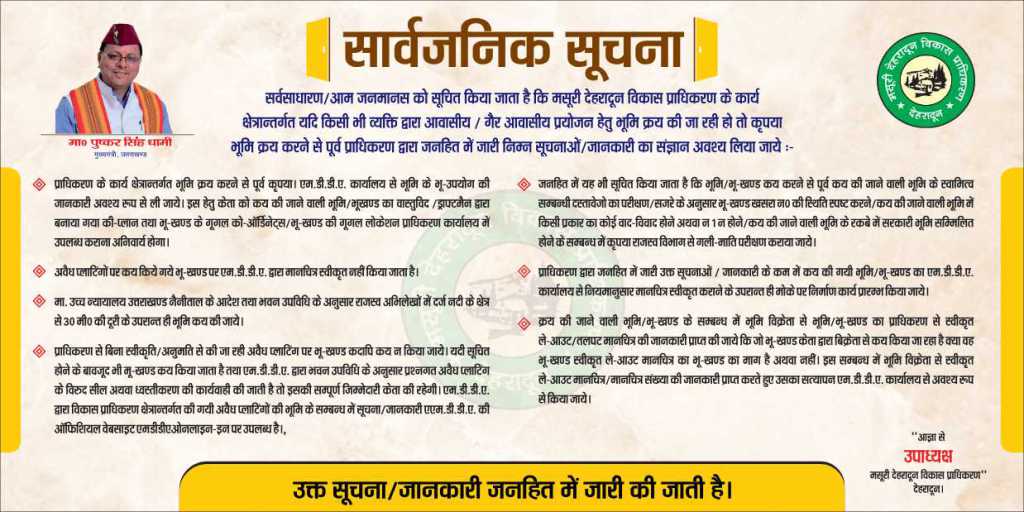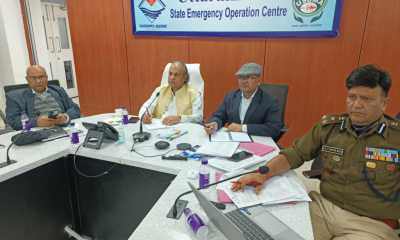आपदा
आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए पृष्ठभूमि और इतिहास को जानना महत्वपूर्ण: गजेन्द्र रौतेला।














संवादसूत्र देहरादून: गजेन्द्र रौतेला के अनुसार, पहाड़ी क्षेत्रों में आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति और प्रवृत्ति का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अनियोजित शहरीकरण और पर्यावरण का क्षरण है, जिसके कारण भूस्खलन, बाढ़ बादल फटने और अन्य प्राकृतिक विपदाएँ बढ़ी हैं।इन आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी भूमि-उपयोग योजना, उच्च-गुणवत्ता वाली निर्माण प्रथाएँ, सामुदायिक जागरूकता और आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRM) पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।
1-आपदा की पृष्ठभूमि और इतिहास –
आपदाएं हमारे जीवन का हिस्सा हो गई हैं | खासकर अतिवृष्टि,बादल फटना ,बाढ़ और भूकंप तो जैसे हमारी नियति हो चुकी हैं | जो कभी दो-चार साल में कभी-कभार हुआ करती थी अब इनकी आवृति हफ्ते से लेकर महीने के अंतराल में कई-कई जगह और कई-कई स्थानों पर एक साथ होना आम बात हो गई है | स्वाभाविक रूप से वैज्ञानिक इसका कारण मानवीय हस्तक्षेप और क्लाइमेट चेंज को बताते हैं | कारण चाहे जो भी हों लेकिन अंततः इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हाशिये पर खड़ा वह अंतिम व्यक्ति हो रहा है जो पहले से ही किसी तरह अपनी ज़िंदगी की बसर कर रहा है | ऊपर से आपदाएं उसके जीवन को पूरी तरह तहस-नहस कर दे रही हैं | जबकि आनुपातिक रूप से देखें तो पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज के लिए वह उतना जिम्मेदार नहीं है लेकिन फिर भी वह इसको भोग रहा है यह एक बड़ी विडंबना है | बावजूद इसके आपदा के पश्चात हमारी व्यवस्था उसकी भरपाई किस तरह से करती है यह किसी छिपा नहीं है | मानवीय गरिमा के अनुरूप उसको राहत सामग्री तक नहीं मिल पाती है ,इसके लिए भी उसे कई जगह भटकना पड़ता है वह भी कई औपचारिकताओं को पूरा करने के बावजूद | प्रबल आपदा प्रभावित क्षेत्र होने के बाद भी हम ऐसा सिस्टम नहीं विकसित कर सके कि पीड़ित व्यक्ति के पास जाकर हम उसे कुछ राहत सामग्री तक दे सकें | एक आपदा पीड़ित के बाहर होती है जो दिखाई देती है और दूसरी आपदा उसके भीतर होती है जो कभी किसी को ना तो दिखाई देती है और ना ही उसका कोई पैमाना है और ना ही उसकी भरपाई |
2-वर्तमान में आपदा –
देश के हिमालयी राज्यों में इस बार आपदा की जो सबसे ज्यादा मार झेली है उनमें हिमाचल और उत्तराखण्ड हैं | हिमाचल में जहाँ मनाली ,शिमला ,मण्डी आदि में प्रकृति ने कहर बरपाया जिसके कारण पंजाब भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित है तो वहीँ दूसरी ओर उत्तराखण्ड में उत्तरकाशी के धराली, चमोली के थराली व घाट-नंदानगर के धुर्मा और कुंतरी गाँव ,पौड़ी के सैंजी और रुद्रप्रयाग के छेनागाड का अस्तित्व ही मिट जाना इसके ताजा उदाहरण हैं | इन आपदाओं में न सिर्फ भौतिक नुकसान हुआ है बल्कि कई लोगों की जान भी गई है | यह दोहरी मार पीड़ितों को बुरी तरह ध्वस्त कर देती है,परिवार पूरी तरह छिन्न-भिन्न हो जाता है, वर्ष 2013 की आपदा के कई उदाहरण आज भी हमारे आस-पास मौजूद हैं | डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में हिमांचल प्रदेश में 476 लोग मारे गए और 1151 करोड़ का नुकसान हुआ | 2022 में 276 मौतें और 939 करोड़ का नुकसान , 2023 में 441 मौतें और 12000 करोड़ रुपए का नुकसान , 2024 में 174 मौतें और 1613 करोड़ का नुकसान हुआ था जबकि उत्तराखण्ड में केवल इस साल हुई आपदाओं ने केदारनाथ आपदा के बाद से सबसे अधिक आर्थिक नुकसान हुआ | बीते अगस्त माह तक 5000 करोड़ रुपए तक इसका आंकड़ा पहुँच गया था | वहीँ दूसरी ओर हिमांचल में 13000 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुक्सान हो चुका है | अगस्त माह तक सिर्फ तीन महीनों में ही हिमांचल में 327 और उत्तराखण्ड में 77 और जम्मू कश्मीर में 132 के मारे जाने के आंकड़े बताते हैं कि यह स्थिति कितनी डरावनी होती जा रही है |
3 -आपदा का प्रभाव-
आपदा का सीधा प्रभाव भौतिक और आर्थिक रूप से प्रत्यक्ष तो दिखाई तो देता है जिससे पूरा परिवार जूझता ही है लेकिन वो अप्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई नहीं देता है अक्सर जो मनोवैज्ञानिक रूप से किसी भी पीड़ित और प्रभावित व्यक्ति पर दूरगामी होता है | इस विषय पर दून विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रो0 राजेश भट्ट जो ट्रॉमा मैनेजमेंट के विशेषज्ञ हैं बताते हैं कि “यह त्रासदी न सिर्फ शारीरिक और आर्थिक होती है बल्कि इसका ट्रॉमा तो कभी-कभी इतना गहरा होता है कि पीड़ित व्यक्ति ज़िंदगी भर इससे उबर ही नहीं पाता अक्सर इसका आंकलन कभी हो ही नहीं पाता खासकर महिलाओं और बच्चों में इसके बहुत से लक्षण दिखाई देते हैं जिसका प्रभाव उन पर अक्सर लम्बे समय तक रहता है |
4- आपदा के कारण और विशेषज्ञों की राय –
अतिवृष्टि और बादल फटने की बढ़ती घटनाओं के बारे में लम्बे समय से विशेषज्ञों की विभिन्न राय आती रही हैं जिसमें एक प्रमुख कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक और अवैज्ञानिक दोहन के साथ-साथ ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज एक प्रमुख कारण है | ईको एंड एनर्जी की एक रिपोर्ट में एनवायरनमेंट जर्नलिस्ट हृदयेश जोशी बताते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार जब धरती का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो बारिश 7 गुना तक बढ़ जाती है | दूसरी तरफ वडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ हिमालयन जियोलॉजी के प्रसिद्ध ग्लेशिओलॉजिस्ट डॉ0 मनीष मेहता जो पिछले एक दशक से लद्दाख में हिमालय की जांस्कार पर्वत श्रृंखला का अध्ययन और अनुसंधान कर रहे हैं,उन्होंने थर्ड पोल लाइव को दिए अपने एक बयान में कहा कि,” हमारे देश में बारिश दो कारणों से होती है पहला कारण है यूरोप से भूमध्यसागर की तरफ से आने वाला पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) जो पाकिस्तान से होते हुए भारत में पहुँचता है और यहाँ बारिश करता है जो की सामान्यतः भारत में सर्दियों की बारिश करता है जबकि इस बार यह क्लाइमेट चेंज की वजह से सर्दियों से पहले ही गर्मियों में पहुँच गया और साथ-साथ ही हिन्द महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण-पश्चिम तट से भी मानसून ने प्रवेश किया दोनों के एक साथ आने से स्वाभाविक रूप से बारिश की मात्रा और अवधि दोनों बढ़ी जिस कारण अतिवृष्टि हुई और कई स्थानों पर भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं हुई जिससे बहुत बड़ी मात्रा में जानमाल का नुकसान हुआ | साथ ही डॉ0 मेहता यह भी कहते हैं कि 24 वर्षों बाद मौसम में यह भी स्थितियां बनी कि पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) उच्च हिमालय को पार करते हुए तिब्बत के पठारों तक जा पहुंचा जिस कारण वहां भी बर्फवारी के साथ-साथ भारी और मोटी बारिश हुई जहाँ कभी सिर्फ बेहद हल्की बारिश और बर्फवारी हुआ करती थी | इसके जिवंत उदाहरण हमारे यहां रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं जहाँ लगातार भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाएं रिकॉर्ड की जा रही हैं मानव समाज के लिए यह बेहद चिंताजनक स्थिति है | वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ भूवैज्ञानिक प्रो0 नवीन जुयाल जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित चारधाम सड़क परियोजना की समीक्षा के लिए गठित हाई पॉवर कमेटी में एक सदस्य भी रहे हैं उनका कहना है कि,” मौसम और पर्यावरण को प्रभावित करने वाले स्थानीय कारक भी बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावी होते हैं जिनमें बेतरतीब और अवैज्ञानिक तरीके से सड़कों को बनाने के लिए पेड़ों का कटान ,बेशुमार बड़े-बड़े हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स का बनना और उनका मक डंपिंग,अनियंत्रित पर्यटन और ट्रैफिक की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है |” डॉ0 जुयाल की इस बात को अपने अनुभवों के आधार पर पुष्टि करते हुए रुद्रप्रयाग जिले के वरिष्ठ पत्रकार और चिपको आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्त्ता रमेश पहाड़ी भी अपनी सहमति जताते हैं | एक तथ्य यह भी गौर किये जाने वाला है कि इस उत्तराखण्ड में इस वर्ष अभी तक जहाँ भी आपदाएं आई हैं मौसम विभाग के अनुसार वहां कहीं भी बादल फटने जैसी घटनाएं दर्ज नहीं हैं क्योंकि देहरादून स्थित मौसम विभाग के मौसम विज्ञानियों के अनुसार बादल फटने की घटना उसे कहा जाता है जब किसी स्थान पर एक घंटे में 100 मिमी0 बारिश हो जबकि रुद्रप्रयाग जिले की छेनागाड़ की आपदा 28-29 अगस्त 2025 के दिन यह पैमाना 48 मिमी0, नंदानगर घाट चमोली की आपदा 17-18 सितम्बर 2025 के दिन 70 मिमी0 और देहरादून के मालदेवता में 15-16 सितम्बर 2025 को यह आंकड़ा 24 घण्टे में 149 मिमी0 रिकॉर्ड किया गया जबकि देहरादून का अभी तक का सबसे अधिक वर्षा का रिकॉर्ड सन 1966 में 487 मिमी0 का दर्ज है | मौसम विभाग केंद्र देहरादून के निदेशक डॉ0 चंद्र सिंह तोमर बताते हैं कि भले ही अधिकांश जगहों पर बादल फटने के जैसे स्थिति न रही हो लेकिन बारिश से होने वाला नुकसान स्थानीय कारकों और वहाँ की भौगोलिक स्थिति पर बहुत अधिक निर्भर करता है |
5- नीति एवं नियोजन –
उत्तराखण्ड के हिमालयी क्षेत्र में प्रति दस वर्ष में होने वाली 1150 किमी0 और 45 दिनों में संपन्न होने वाली अस्कोट आराकोट अभियान 2024 की यात्रा में हमने कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जिले के अंतिम गाँव पांगू अस्कोट से उत्तरकाशी जिले के आराकोट गाँव तक देखा कि पहाड़ के गाँवों को सड़कों से जोड़ने की बेहद बुनियादी आवश्यकता तो है लेकिन जिस अवैज्ञानिक और बेतरतीब तरीके से सड़कों को काटा जा रहा है और उनके लिए जिस तरह से अधिकाँश जगहों पर गैरजरूरी तरीके से जंगलों का कटान और मलबे का निस्तारण किया जा रहा है वह भी इन दूरस्थ गाँवों में आपदा और भूस्खलन का बड़ा कारण बन रहे हैं | इसके जीवंत उदहारण हमें चमोली जिले के नंदानगर घाट विकासखण्ड के सीक और झिंझी-पाणा-इराणी गाँव की सड़क के निर्माण के दौरान देखने को मिला जहाँ न डी0पी0आर0 के मुताबिक निर्माण कार्य हो रहा था और न मलबे निस्तारण | यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और एन0जी0टी0 ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जिन जिलेटिन की कारतूसों से विस्फोट को पहाड़ों में प्रतिबंधित किया हुआ है उसे भी बेहद क्रूर तरीके इस्तेमाल होते हुए प्रत्यक्ष देखा है | यही स्थिति विभिन्न हाइड्रोप्रोजेक्ट्स की भी है | सरकारी स्तर पर इनके निर्माण कार्यों को धरातल पर मॉनिटर करने वाला कोई भी नहीं दिखाई देता | दरअसल इन कंपनियों के तार कहीं न कहीं सत्ता से जुड़े हुए होते हैं जिससे स्थानीय प्रशासन भी इन झंझटों में पड़ने से दूरी बनाये रखने में ही अपना हित समझते हैं | दूसरी तरफ इन कंपनियों का कहना होता है कि हमने पर्यावरण के नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार के वन विभाग को करोड़ों की कीमत चुकाई है |
6-परिणाम एवं निष्कर्ष –
कागजी स्तर पर सब कुछ सुनहरा होने के बावजूद भी आज जगह-जगह रौखड़ों की भरमार दिखाई देती है यह भी एक यथार्थ है जिसकी भरपाई अंतिम पंक्ति पर खड़ा वह आम व्यक्ति चुका रहा है जो मजबूरीवश ही सही पहले से ही पलायन की मार झेल रहे पहाड़ के गाँवों के अस्तित्व को बचाये हुए है | जिसका ताजा उदाहरण अभी देहरादून में आई भीषण बाढ़ से मची तबाही प्रत्यक्ष है | सरकार को चाहिए कि दोहरी मार झेल रहे इन पहाड़वासियों का भी ख्याल रखे ताकि क्लाइमेट चेंज और तथाकथित विकास के इस मॉडल से आज पहाड़ से होते हुए ये आपदाएं मैदान तक पहुँच गई हैं उन्हें रोका या कम किया जा सके | यह बात सभी को समय रहते समझ आ जानी चाहिए कि यदि पहाड़ सुरक्षित होंगे तभी मैदान भी सुरक्षित रहेंगे |